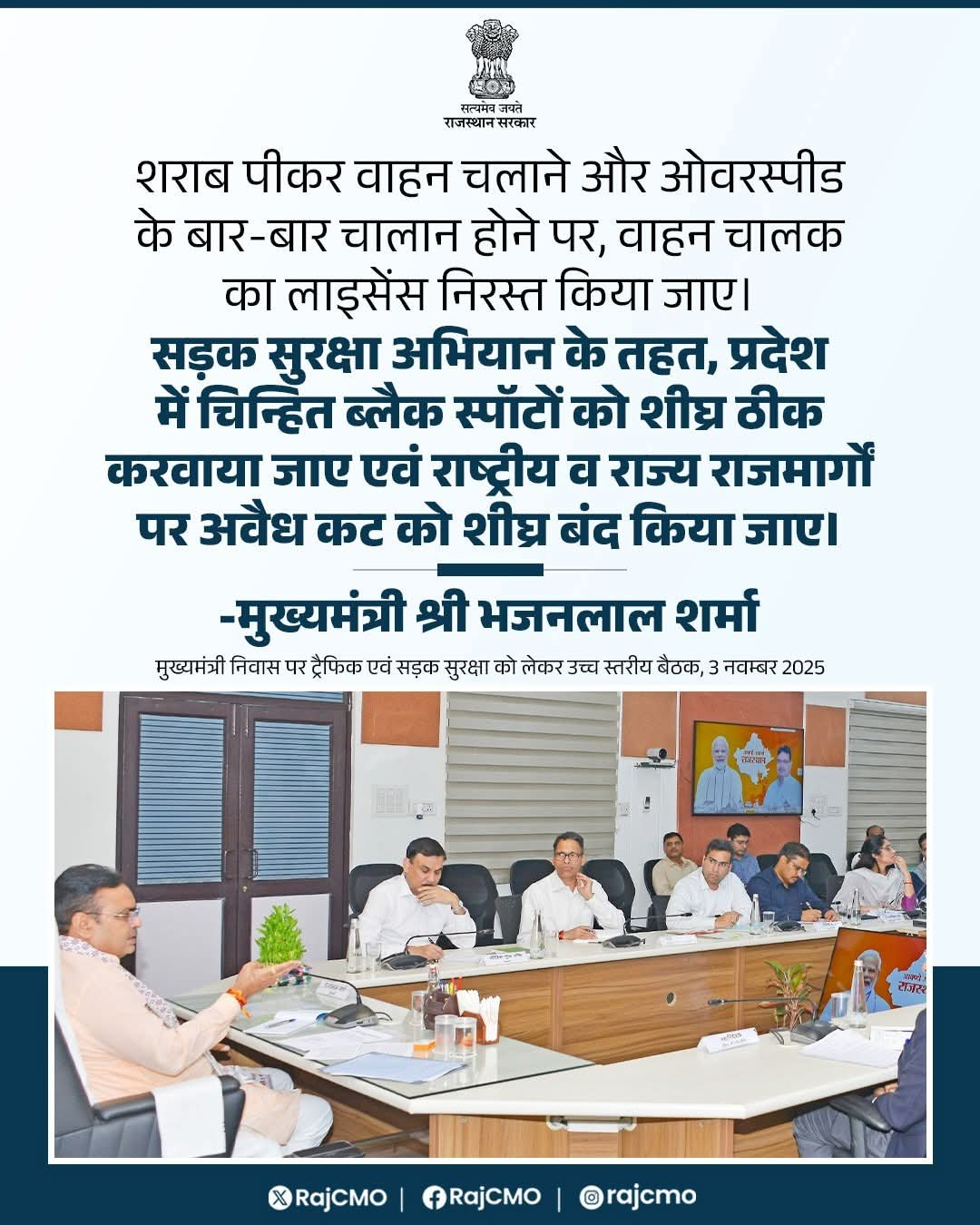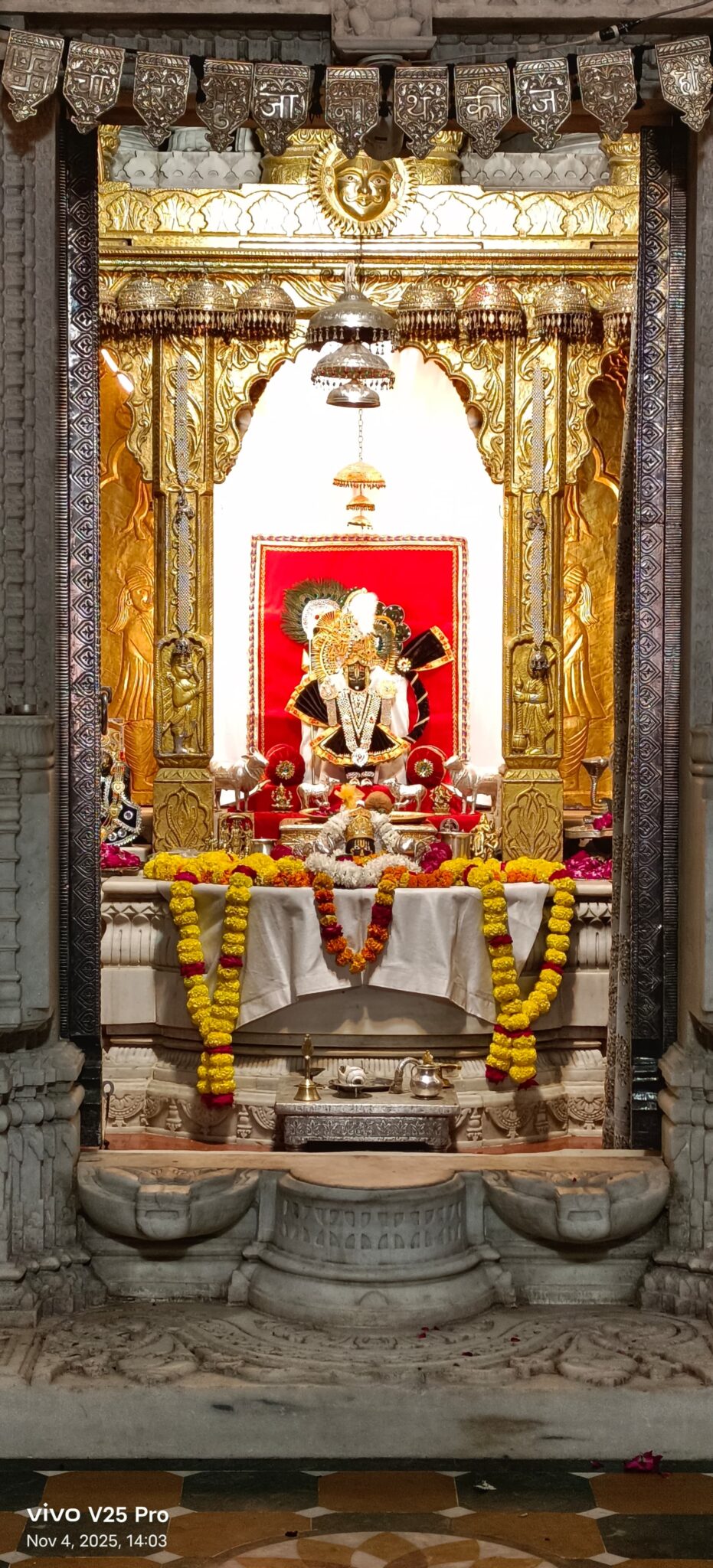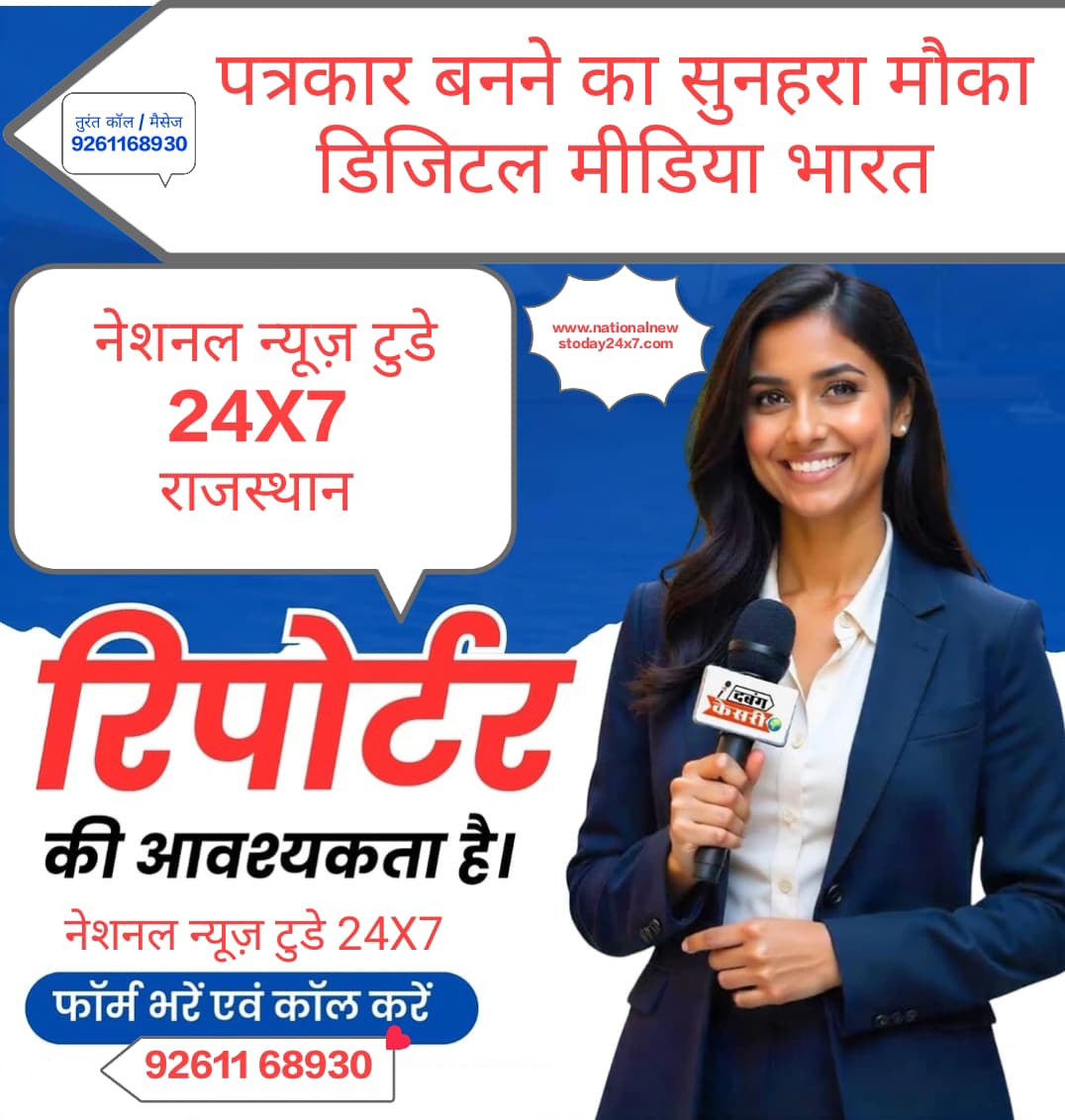
“प्रकृति से प्रगति तक: श्रीमद्भगवद्गीता में पर्यावरणीय नैतिकता का प्रतिपादन”
लेखक – डॉ. बृजेश कुमार साहू
आज जब वैश्विक मंच पर पर्यावरण संरक्षण की चर्चा नीति और विज्ञान के स्तर पर होती है, श्रीमद्भगवद्गीता ने उसी चेतना का आध्यात्मिक व दार्शनिक आधार प्रस्तुत किया था। गीता केवल मोक्ष या कर्म का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन और प्रकृति के संतुलन का शाश्वत विधान भी है। पर्यावरण (Environment) वह समग्र तंत्र है जो मानव, पशु, वनस्पति, जल, वायु, पृथ्वी और अंतरिक्ष सभी को जोड़ता है। यह केवल भौतिक तत्त्वों का समूह नहीं, बल्कि जीवन का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार है। आज जब मानव ने विज्ञान और तकनीक की सहायता से प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया है, तब उसका असंतुलन पूरे विश्व के लिए संकट बन गया है — जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, तापवृद्धि और जैव विविधता का विनाश इसके परिणाम हैं। श्रीमद्भगवद्गीता, जो भारतीय जीवन-दर्शन का सार है, इन समस्याओं का समाधान अपने दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। गीता में पर्यावरण को केवल भौतिक सत्ता नहीं, बल्कि दैवी शक्ति (Divine Energy) के रूप में देखा गया है। गीता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भगवान श्रीकृष्ण गीता में प्रकृति के दो रूपों का वर्णन करते हैं —
1. अपरा प्रकृति (स्थूल पदार्थ रूपी प्रकृति)
2. परा प्रकृति (जीव रूपी चेतन शक्ति)
आदि-शंकराचार्य अद्वैत का दृष्टिकोण वह प्रकृति को अपरा प्रकृति के रूप में समझते हुए कहता है कि परम-तत्त्व से संसार का अभ्युदय और उद्गम होता है। आदि-शंकराचार्य का अद्वैत- दर्शन प्रत्यक्ष संरक्षणवादी नीति नहीं देता, पर समान चेतना का संदेश मनुष्य में प्रकृति के प्रति सहानुभूति और हिंसा-विरोध उत्पन्न कर सकता है — क्योंकि परम में एकता का अनुभव सब में करुणा जगाता है।
यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार — मेरी अपरा (भौतिक) प्रकृति है, परन्तु इससे भिन्न एक परा (चेतन) प्रकृति भी है जो इस जगत को धारण करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह पृथ्वी के तत्वों का अद्भुत वर्णन है — पंचमहाभूत जो आज भी “ईकोलॉजिकल एलिमेंट्स” माने जाते हैं। गीता इन तत्वों को जीवंत, आपस में जुड़े और संतुलित तत्त्व मानती है। आधुनिक इकोसिस्टम (Ecosystem) की संकल्पना से मेल खाता है। आधुनिक पर्यावरण विज्ञान भी यही कहता है कि हर तत्त्व एक-दूसरे पर निर्भर है; यदि एक का संतुलन बिगड़ा, तो संपूर्ण जैविक तंत्र प्रभावित होता है। संयम और संतुलन का सिद्धांत पर गीता का वैज्ञानिक संदेश है — जीवन में संयम और संतुलन व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए भी आवश्यक है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इसे Sustainable Development कहा जाता है — “इतना ही उपभोग करो, जितना प्रकृति पुनः उत्पन्न कर सके।”
अरविंदो गीता को “जीवन का दिव्यीकरण” की पुस्तक मानते हैं। वे प्रकृति-परिवर्तन को आध्यात्मिक उन्नयन से जोड़ते हैं । पर्यावरणी निहितार्थ: सधा हुआ वैज्ञानिक-आध्यात्मिक संयोजन; तकनीक और विज्ञान तब सुरक्षित हैं जब वे प्रकृति के दिव्यकरण और पुनर्संतुलन के उद्देश्य से हों।
गीता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण : प्रकृति एक जीवंत तंत्र भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा —“भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ” (गीता 9.8) अर्थात् सारा सृष्टि-समूह प्रकृति के द्वारा ही संचालित होता है। आधुनिक पारिस्थितिकी (Ecology) की मूल धारणा से मेल खाता है — कि सृष्टि एक पारस्परिक तंत्र है, जिसमें प्रत्येक तत्व का अपना स्थान और कार्य है। गीता में ‘प्रकृति’ को दिव्य ऊर्जा कहा गया है, जो पंचमहाभूतों — पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश — के संतुलन से निर्मित है। यह वही वैज्ञानिक दृष्टि है, जिसे आज “इको-सिस्टम बैलेंस” कहा जाता है।
श्रीमद्भगवद्गीता का कर्मयोग केवल व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं, बल्कि पर्यावरणीय उत्तरदायित्व का भी संदेश देता है —“यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः।” (गीता 3.9) यज्ञ अर्थात् लोक-कल्याण के लिए किया गया कर्म ही बंधन-मुक्त है।यहाँ ‘यज्ञ’ केवल अग्निहोत्र नहीं, बल्कि व्यापक अर्थ में सामाजिक-प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक है। जब मनुष्य अपने कर्मों को पृथ्वी, जल, वनस्पति और जीव-जगत के कल्याण से जोड़ता है, तभी सच्चा पर्यावरण-धर्म निभाता है।
स्थायी विकास की दिशा भगवान कृष्ण कहते हैं केवल आवश्यक उपभोग ही शुद्ध है। प्रकृति का अंधाधुंध दोहन पाप का कारण बनता है। यही आज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट (Sustainable Development) सिद्धांत है — ‘जितनी आवश्यकता, उतना ही उपयोग।’ प्रकृति के विरोध में श्रीमद्भगवद्गीता में स्पष्ट चेतावनी दी गई है —“अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्।” (गीता 16.18) ये दैत्यस्वभाव के लक्षण हैं जो मानव को विनाश की ओर ले जाते हैं। आधुनिक प्रदूषण, वनों की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग इन्हीं दैत्य-स्वभावों के फल हैं। गीता के अनुसार, जब मनुष्य अहंकारवश प्रकृति पर अधिकार जमाना चाहता है, तो संतुलन नष्ट होता है और परिणाम स्वरूप आपदाएँ जन्म लेती हैं।
प्रकृति का संरक्षण: एक नैतिक कर्तव्य (Environmental Protection as Moral Duty)
रामानुज प्रकृति और जीव दोनों को ईश्वर की अन्तर्निहित शक्ति मानते हैं: पुरुष-प्रकृति का द्वन्द्व, पर प्रकृति का अस्तित्व और कार्य ईश्वर की अनुग्रहशक्ति से नियंत्रित है। रामानुज गीता के गहन व्यावहारिक अर्थ पर ज़ोर देते हैं — कर्म, यज्ञ और समाज-हित का समन्वय। पर्यावरणी निहितार्थ: रामानुज के सन्दर्भ में प्रकृति का संरक्षण ईश्वर-सेवा का भाग है; यज्ञ/कर्म के माध्यम से प्रकृति-पर्यावरण को समुचित रूप से पोषित करने का नैतिक दायित्व बनता है। यह दृष्टि प्रत्यक्ष-नीतिगत संरक्षण और सामुदायिक प्रबंधन का बौद्धिक आधार देती है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं — “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।” (2.47). प्रकृति का संरक्षण केवल स्वार्थ या लाभ के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्यभाव से किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण “पर्यावरणीय नैतिकता (Environmental Ethics)” का सबसे उच्च रूप है। आधुनिक विज्ञान भी अब “Ethical Ecology” की बात करता है मानव का हर वैज्ञानिक प्रयास प्रकृति के कल्याण के अनुरूप होना चाहिए। ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता है। ज्ञानी व्यक्ति सभी में एक समान ईश्वर को देखता है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से Biospheric Equality का सिद्धांत है — हर जीव का अस्तित्व समान रूप से आवश्यक है।यह दृष्टि जैव विविधता (Biodiversity) के संरक्षण की मूल चेतना है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार, पृथ्वी एक Living System है। गीता इसे बहुत पहले ही “जीवभूतां परा प्रकृति” कहकर स्पष्ट कर चुकी है। जहाँ आधुनिक विज्ञान Cause and Effect के सिद्धांत पर चलता है, वहीं गीता “कर्म और यज्ञ” के माध्यम से Balance and Harmony का वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत करती है। दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि संतुलन ही अस्तित्व का आधार है। यदि यह संतुलन टूटेगा, तो संपूर्ण प्रणाली (System) धवस्त हो जायेगी । श्रीमद्भगवद्गीता के दृष्टिकोण से पर्यावरण का संरक्षण वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अनिवार्यता है। प्रकृति ईश्वर की अभिव्यक्ति है, उसका संतुलन यज्ञ और संयम से बनता है,और उसका संरक्षण मानव का सर्वोच्च कर्तव्य है। इस प्रकार गीता का संदेश आज के वैज्ञानिक युग में भी उतना ही प्रासंगिक है ।
“राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय चिंतन की उस परंपरा को पुनर्स्थापित करता है जिसमें प्रकृति और संस्कृति का संबंध अविभाज्य माना गया है। संघ का दृष्टिकोण ‘सहजीवन’ और ‘संवर्धन’ की भावना पर आधारित है, जो भोग नहीं, योग की चेतना को प्रोत्साहित करता है। संघ के कार्यकर्ता वृक्षारोपण, जल-संरक्षण, स्वच्छता अभियान और ग्रामोदय जैसे कार्यों में सक्रिय भागीदारी द्वारा “प्रकृति से प्रगति” के आदर्श को मूर्त रूप देते हैं। यह दृष्टि पश्चिमी विकास मॉडल की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति से भिन्न, एक आध्यात्मिक पर्यावरणवाद (Spiritual Environmentalism) की दिशा प्रस्तुत करती है।